फिल्में कभी सीधे-सीधे साहित्य या किताबों से एडाप्ट की जाती हैं, कभी केवल प्रेरित होती हैं, कभी अनजाने में, इशारे में कहीं जुड़ जाती हैं, और कहीं-कहीं चुराई भी जाती हैं।
आज इस मसले पर दो ताजा फिल्मों का हवाला लेकर बात करने का मन है। और मैं यह बात कहने का साहस इसलिए कर रहा हूं कि साहित्य और सिनेमा दोनों की गलियों से थोड़ा वैध-अवैध रिश्ता मेरा भी है।
अमेजोन प्राइम पर रिलीज हुई शुजीत सरकार – जूही चतुर्वेदी की ‘गुलाबो सिताबो’ ठहराव और गति, प्रेम और लालच, वय और संवेदना के बीच जीवन के धागों की सिम्फनी है, जिसमें भारतीयता का रस है। एक तरह से देखा जाए तो ‘गुलाबो सिताबो’ शुजीत और जूही ही हैं। ऐसी निर्देशक-लेखक की जोड़ियां दुर्लभ हैं, पर अभीष्ट हैं। 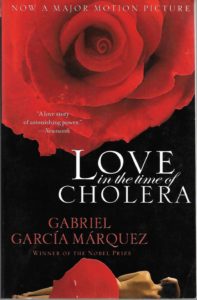 फिल्म का अंत पिछली सदी के महान कथाकार गेब्रिअल गार्सिया मार्खेज के उपन्यास ‘लव इन द टाइम ऑफ कॉलेरा’ के अंत की याद दिलाता है, दोनों के अंत की चर्चा करके दोनों के पाठकीय-दर्शकीय सुख से आपको वंचित करने का अपराध नहीं करूंगा। बस इतना जरूर कहना चाहिए कि मार्खेज प्रेम की उत्तरजीविता और देह-मन की गुत्थियों को नए नजरिए से देखते विश्लेषित करते हैं, ‘गुलाबो सिताबो’ का अंत इशारे में वहीं पहुंच जाता है। कहावत है कि कविता इशारे का आर्ट है, मेरी राय में सिनेमा कविता से आगे का इशारे का आर्ट है, और उस स्तर पर आकर वह खालिस लिटरेचर ही हो जाता है, तभी एक विचार हमारे समय में जमीन पा गया है कि सिनेमा इज द न्यू लिटरेचर।
फिल्म का अंत पिछली सदी के महान कथाकार गेब्रिअल गार्सिया मार्खेज के उपन्यास ‘लव इन द टाइम ऑफ कॉलेरा’ के अंत की याद दिलाता है, दोनों के अंत की चर्चा करके दोनों के पाठकीय-दर्शकीय सुख से आपको वंचित करने का अपराध नहीं करूंगा। बस इतना जरूर कहना चाहिए कि मार्खेज प्रेम की उत्तरजीविता और देह-मन की गुत्थियों को नए नजरिए से देखते विश्लेषित करते हैं, ‘गुलाबो सिताबो’ का अंत इशारे में वहीं पहुंच जाता है। कहावत है कि कविता इशारे का आर्ट है, मेरी राय में सिनेमा कविता से आगे का इशारे का आर्ट है, और उस स्तर पर आकर वह खालिस लिटरेचर ही हो जाता है, तभी एक विचार हमारे समय में जमीन पा गया है कि सिनेमा इज द न्यू लिटरेचर।
‘गुलाबो सिताबो’ में हवेली का मैटाफर गुरूदत्त-विमल मित्र की ‘साहेब बीवी और गुलाम’ का रचनात्मक, युक्तिसंगत विस्तार लगता है। ‘गुलाबो सिताबो’ में हवेली के इस मैटाफर को जीवंत करने में शुजीत का साथ सिनमैटोग्राफर अवीक मुखोपाध्याय ने कमाल तरीके से दिया है। यह मैटाफर का खेल देखा जाए तो साहित्यिक ही है।
मिथकीय विस्तार, संवेदना और भाषा के लिहाज से भारत या कहिए हिंदुस्तान यहां फिल्म के शुरू से आखिर तक धड़कता है। फिल्म दिखने में वोकल है, जहां-जहां बीच में नि:शब्द है, फिल्म का जादुई यथार्थ वहीं छुपा है। वही जादुई यथार्थ जिसके मसीहा मार्खेज कहे गए हैं।
‘चोक्ड’ नेटफ्लिक्स पर आई है, पूरी तरह से अनुराग कश्यप की फिल्म है। यानी उनके स्टाइल और कम्फर्ट ज़ोन की फिल्म है, पर बिना गाली और अंतरंग दृश्य के। राइटर टर्न्ड डायरेक्टर की फिल्म में राइटिंग क्रेडिट्स में डायरेक्टर क्रेडिट शेयर न करे, ऐसा दुर्लभ होता है, इस फिल्म में ऐसा संयोग बन पड़ा है।
फिल्म को मैं सहजता के सौंदर्य का पाठ कहना पसंद करूंगा। विजुअल्स में कहानी कहने के तरीके में प्रयोग भी है, परंपरागत किस्सागोई भी। पॉलिटिक्स का महीन धागा सब्जी में हींग सा महक रहा है। वही हींग जिसके लिए बाबा नागार्जुन कहते थे कि साहित्य में विचार हींग की तरह ही आना चाहिए, सब्जी में हींग ज्यादा पड़ जाए तो सब्जी कड़वी हो जाती है। 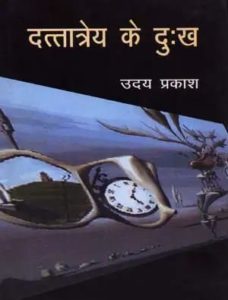 इसी हींग की तरह, फिल्म देखते हुए हिंदी के मार्खेज यानी उदयप्रकाश की कहानी ‘दिल्ली की दीवार’ याद आती रहती है, अनुराग हिंदी साहित्य से गहरा अनुराग रखते ही हैं। दिल्ली की दीवार पर पिछले साल मराठी में अमोल गोले की नशीबवान फिल्म भी आई थी। दिल्ली की दीवार में एक सफाई वाले की झाड़ू का पिछला हिस्सा जब दिल्ली की एक दीवार पर अनायास ठोका जाता है तो दीवार से अथाह पैसा निकलने लगता है, दिल्ली के भ्रष्टाचार का अकूत धन।
इसी हींग की तरह, फिल्म देखते हुए हिंदी के मार्खेज यानी उदयप्रकाश की कहानी ‘दिल्ली की दीवार’ याद आती रहती है, अनुराग हिंदी साहित्य से गहरा अनुराग रखते ही हैं। दिल्ली की दीवार पर पिछले साल मराठी में अमोल गोले की नशीबवान फिल्म भी आई थी। दिल्ली की दीवार में एक सफाई वाले की झाड़ू का पिछला हिस्सा जब दिल्ली की एक दीवार पर अनायास ठोका जाता है तो दीवार से अथाह पैसा निकलने लगता है, दिल्ली के भ्रष्टाचार का अकूत धन।
अनुराग की सब फिल्में मुझे पसंद नहीं आतीं, यानी उनकी फिल्मों की केवल उनका नाम देखकर आंख मूंदकर तारीफ नहीं कर पाता, पर यह फ़िल्म देखनी चाहिए। यह हमारे सिनेमा के कद का ऊर्ध्व विस्तार करने वाला सिनेमा है, शायद इसलिए कि साहित्यिक गरिमा, वैचारिक हींग और रिलवेंस का तानाबाना इस फिल्म को अलग अर्थभंगिमा देते हैं।
साहित्य और जीवन से गहरा अनुराग रखने वाले फिल्मकारों के सिनेमा में सायास-अनायास साहित्य की अनुगूंजें आती रही हैं, आती रहेंगी। पोस्ट कोरोना डिजिटल रिलीज के दौर में भी साहित्य से प्रेरित, दुष्प्रेरित होना सिनेमा को नए पंख और नई उड़ानें देगा, ऐसा मेरा यकीन है।
